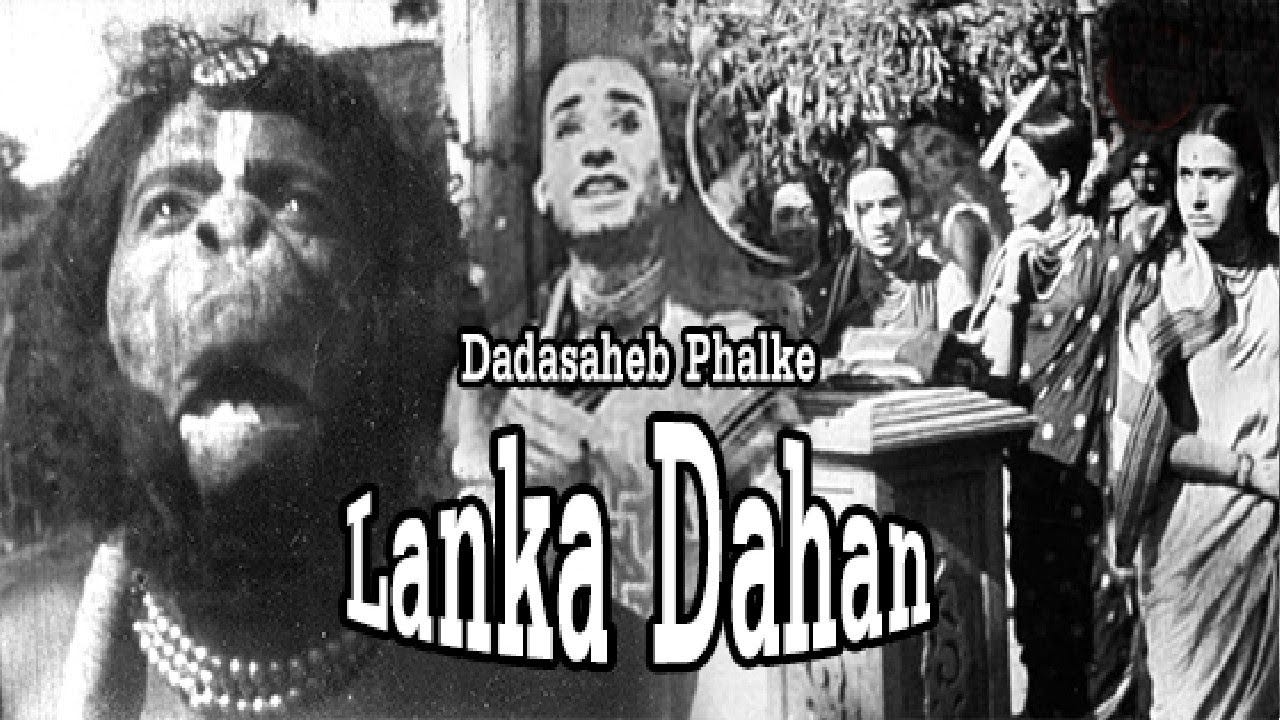लाइट्स-कैमरा-वुमन
माँ ने बताया था “ खून की धार ठीक वैसे ही उछली थी जैसे पानी से भरी पन्नी में छेद कर दो” मुझे आज भी वो याद है जैसे कुरोसावा की “सेवन समुराई” या टैरंटीनो की “किल बिल” में खून बहा था
सिनेमा के इतिहास में महानतम एडिटरों में से एक थैल्मा स्क़ूनमाकर, जो लगभग पिछले पचास सालों से मार्टिन स्कॉर्सेसी की महानतम फ़िल्मों को एडिट टेबल पर दिशा देते आ रही हैं, जिनमें रेजिंग बुल से लेकर गुड फैलाज़ शामिल हैं
उनसे सवाल पूछा गया
“एक स्त्री कैसे इतनी हिंसक फ़िल्मों की एडिटिंग कर सकती है?” उन्होंने जवाब दिया “आह! पर वो फ़िल्में तब तक हिंसक नहीं होती, जब तक मैं उन्हें एडिट नहीं करती”
स्क़ूनमाकर के जवाब में एक अनदेखा आत्मविश्वास था और सवाल में छुपी मैस्क्युलिनिटी के इस रवय्ये को लेकर एक हताशा थी।
जिस तरह स्क़ूनमाकर दृश्यों को जोड़कर, काटकर और छाँटकर सिनेमा के पर्दे के लिए कहानियाँ तैय्यार करती हैं उसी तरह घर के भीतर भी हमेशा दादी-नानी बरसो पुराने क़िस्सों को जोड़ कर, छाँट कर, नयापन देकर सुनाया करती थी, कभी लंका से लौटने के बाद सीता की अग्निपरीक्षा तो कभी घर की बड़ी खिड़कियों में झूलते पर्दे, सोलह हाँथ की साड़ियाँ, ऊन के स्वेटर, कभी घर की छत पर पापड़ डालते वक्त बंदरों का आ धमकना और फिर लट्ठ लेकर दादी का उन्हें डराना जब तक घर का कोई मर्द नहीं आता था, बंदर भागते नहीं थे।
माँ की कहानियों में घर की दीवारें थी, अपनी छोटी बहनों को स्कूल के लिए तैय्यार करना था, और सिलायी मशीन का वो क़िस्सा था जिसमें एक बार उनकी ऊँगली मशीन की सुई की गिरफ़्त में आ गयी थी, माँ ने बताया था “ खून की धार ठीक वैसे ही उछली थी जैसे पानी से भरी पन्नी में छेद कर दो” मुझे आज भी वो याद है जैसे कुरोसावा की “सेवन समुराई” या टैरंटीनो की “किल बिल” में खून बहा था
घर के आदमी रावण वध ऐसे सुनाते थे जैसे खुद कोई बड़े ऐक्शन डायरेक्टर हों, कहा-सुनी से लेकर मार धाड़ सब बहुत डिटेल्ड था । उन क़िस्सों में एक अजीब सा अड्वेंचर और मिस्टरी थी, बर्बरता थी जैसे अनुराग कश्यप की फ़िल्मों में होती है जहां किरदार दूसरे किरदार का पत्थर से सर कुचल देता है और पत्थर के हड्डियों से टकराने की आवाज़ बेचैन कर देती है।
मैंने सिनेमा को हमेशा घर या कमरे के भीतर कम घटता हुआ पाया और बाहर ज़्यादा, सिनेमा में पिता के बताए हुए क़िस्से ज़्यादा मिले माँ के सुनाए हुए कम, घर की औरतों की कहानियों का स्थायी भाव भी मेरे अनुभव किए हुए सिनेमा से नदारद रहा, ड्रामा और दृश्यों की पेसिंग में सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ता रहा जैसे पिता की बातें
तो माँ और नानी के अनुभव, हज़ारों लाखों औरतों का जीवन बड़े पर्दे पर क्यों नहीं दिखता था, सवाल से ज़्यादा ये मेरे मन में कौतूहल का भाव ज़्यादा है।
किसी पुरानी मैगज़ीन में छपे एक साक्षात्कार में एक प्रोड्यूसर से सवाल किया गया था की कहानियाँ हमेशा नायक की ही क्यों बनती हैं, नायिका की क्यों नहीं? प्रोड्यूसर का जवाब लगभग कुछ ऐसा ही था की “जिस दिन औरतें सिनेमा घर का टिकट अपने पैसे से ख़रीदेंगी, हो सकता है की फ़िर उसे नायिका प्रधान कहानी बड़े पर्दे पर देखने मिल जाए”
उस समय तक फ़ॉर्मल सेक्टर में वुमन वर्क फ़ोर्स के आँकड़े बहुत कमजोर थे, आज आँकड़े कुछ और हैं पर फिर भी उस प्रोड्यूसर की बात को सच होने में कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है।
बचपन की एक दोपहर, नैशनल टीवी पर कोई फ़िल्म दिखायी ज़ा रही थी, ओम् पूरी (अनंत) फ़िल्म के नायक हैं, जिसमें अमरीश पूरी उनके पिता का किरदार निभाते हैं और स्मिता पाटिल (ज्योत्सना) नायिका का किरदार, और सदा शिव आम्रपुरकर विलन के किरदार में थे
पहली बार किसी नायिका को देख़ कर मै अचंभित रह गया था, उनके पास अपनी आवाज़ थी, और वो “नहीं” बोलना जानती थी, नायक का किरदार ज़ंजीर के ऐंग्री यंग मैन जैसा ही था पर अमिताभ जैसा हीरो नहीं था, वो वैसा ही दिखा जैसे पिता दिखा करते थे। फ़िल्म में कुछ था जो समझ के परे था पर किसी अनजान सच के बहुत पास जिस से मेरा सामना उस उम्र नहीं हुआ था। फ़िल्म में एक दृश्य में ओम् पूरी, स्मिता पाटिल के साथ एक रेस्टौरेंट में बैठे हुए हैं, स्मिता पाटिल के पास एक कविता की किताब है, ओम् पूरी उस किताब से एक पन्ना निकाल कर पढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे उस कविता को पढ़ते हुए उनकी आवाज़ गम्भीर और चिंतित हो उठती है,
कैमरा कुछ देर उन पर रहता है फिर एक कट के साथ ज्योत्सना की आँखों पे जाता है, उनकी नज़र जैसे अनंत के समूचे व्यक्तित्व को खंगाल लेती हैं
कविता पूरी पढ़ पाने के बाद अनंत का शायद उसी सच से सामना होता है जिसे मैं बचपन में नहीं समझ पाया था।
दोनो किरदार रेस्टौरेंट से बाहर निकल कर बस से अपने अपने गंतव्यों पर निकल जाते हैं, बस में खड़ा एक आदमी ज्योत्सना को बार बार छूता है, जैसे ही अनंत को इस बात का इल्म होता है वो उस आदमी को पीटने लगते हैं, फिर उसे बस से उतार कर उसे और पीटते हैं, पूरे दृश्य में स्मिता उन्हें रोकने की कोशिश करते रहती हैं
“फ़िल्म अर्धसत्य का एक दृश्य”
अनंत जिस तरह उस आदमी को पीटते हैं उसमें सिर्फ़ क्रोध नहीं रहता है, आदर्शवाद को अपना कर जीवन जीने के कामना करने वाले आदमी की हताशा भी होती है, उनके बचपन में आत्म सात की हुई पिता की हिंसा भी लिप्त होती है ।
जिस दृश्य में अनंत कविता पढ़ रहा होता है, वहाँ आदमी के कहे हुए शब्द और औरत की आँखें एक साथ आपसी सहमति से अपना काम कर जाते हैं। “अर्ध सत्य” जो पुरुषों के भीतर वास करती हिंसा, उनके पौरुश्त्व और सिस्टम की शिथिलता को एक बहुत ही तीक्ष्ण दृष्टि से खंगालकर मन को व्याकुल कर देती है और मर्दानगी को अपने चरम पर ले जाकर मर्दानगी की ही आलोचना करते हुए आपको अपने अर्ध सत्य से सामना करने के लिए विवश करती है, ये फ़िल्म कुछ और भी हो सकती थी अगर इसके एडिट टेबल पर एक औरत ना बैठी होती। रेणु सलुजा उस दशक में अपनी कला का लोहा मनवा रही थी जब इंडस्ट्री पूर्णतः एक हिसंक मेल गेज से लिप्त थी।
नज़रिए और सोच की बात सिर्फ़ कहानियों तक ही सीमित नहीं है, तकनीक तक भी पहुँच जाती है
हॉलीवुड के शुरुआती दौर में नायक और नायिका के लिए लाइटिंग टेकनीक में भी अंतर होता था जिसे आज मैस्क्युलिन फ़ेमिनिन लाइटिंग भी कह सकते हैं।इस दौर में किरदारों को रोशन करने के लिए पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी के सिद्धांत इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें मुख्यतः थ्री पॉइन्ट लाइटिंग का इस्तेमाल होता था।
की-लाइट जिसे किरदार के चेहरे के एक तरफ़ रख कर रोशन किया जाता था, फ़िल लाइट जिसे चेहरे के दूसरी तरफ़ मूलतः पैंतालीस डिग्री के कोण पे रखा जाता था जिससे की लाइट के कारण चेहरे पर पड़ रही परछायी को फ़िल किया ज़ा सके या छुपाया ज़ा सके और तीसरी, किरदार के पीछे रखी बैक लाइट जो किरदारों को बैक्ग्राउंड से अलग करती थी यानी उभरा हुआ दिखाती थी
नायक और नायिका, दोनो पर इसी तरह प्रकाश डाला जाता था अंतर इतना होता था की नायक पर हार्श-लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता था, की लाइट, फ़िल लाइट और बैक लाइट के बीच contrast ज़्यादा होता हो जिस से उनके चेहरे और उभर के आता था वहीं नायिका के लिए सॉफ़्ट डिफ़्यूज़्ड लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे उनके चेहरे को एक ग्लो मिलता था, चेहरे पर किसी भी निशान को छुपाने के लिए ज़्यादा मेक उप और ज़्यादा फ़्रंटल लाइट का इस्तेमाल होता था और बालों को उभारने के लिए बैक लाइट, जैसे नायिका एक दिव्य हेलो साथ लिए चलती हो ।
उस समय भारत में दादा साहेब फाल्के राजा हरीशचंद्र, लंका दहन और मोहिनी भस्मासुर जैसे धार्मिक फ़िल्में बना रहे थे, इस दौर में सिनेमा में काम करना औरतों के लिए किसी टैबू जैसा था, तो अधिकतर कहानियों की महिलाओं के किरदार पुरुष ही अदा किया करते थे।
एक दो दशक बीतने के बाद यही तकनीक भारतीय सिनेमा ने अपनायी, नायिका का शांत सुंदर प्रज्ज्वलित चेहरा और उनके पीछे प्रकाश का हेलो वास करता था, हमारे यहाँ औरतों को औरत कम पर माँ, बहन, पत्नी या देवी का दर्जा सदियों को दिया गया है, सिनेमा उस मान्यता को ही मूरत कर रहा था।
हालाँकि विश्व सिनेमा के इतिहास में औरतें हमेशा से ही सिनेमा का हिस्सा रही, 1894 में एडिसन ने एक आदमी की छींक रिकोर्ड की, 1895 में लूमीयर ने फ़ैक्टरी से निकलते हुए मज़दूरों को रिकोर्ड किया, इन सभी रेकोर्डिंज़ को तकनीकी प्रगति माना जा सकता है जिसमें रोज़मर्रा का जीवन दर्ज करने की क्षमता है पर काल्पनिकता या कहानी जैसा क़ुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक एक साल बाद फ़ोटोग्राफ़ी स्टूडियो में काम करने वाली फ़्रेंच मूल की ऐलिस-गी-ब्लाशे ने 1896 में “कैबेज फ़ेयरि” नाम की एक फ़ैंटसी फ़िल्म बनायी जिसमें एक परी पत्तागोभी के पत्तों से बच्चे प्रकट कर सकती थी, बहुत से फ़िल्म क्रिटिक्स या फ़िल्म के जानकार इसे सिनेमा के इतिहास में पहली काल्पनिक फ़िल्म का दर्जा भी देते हैं। ऐलिस इस फ़िल्म की राइटर, सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर थी
वहीं 191३ में लूई वेबर नाम की अमेरिकन फ़िल्मकार उस समय अबॉर्शन, बर्थ कंट्रोल और कैपिटल पनिश्मेंट ज़ैसे थीम्ज़ को आधार बना कर फ़िल्में बना रही थी, पर बात सिर्फ़ उनकी सामाजिक सजगता तक ही सीमित नहीं थी, तकनीक के मामले में भी वो सिनेमा को इवॉल्व होने में मदद कर रही थी, उन्हें उनकी शॉर्ट फ़िल्म “सस्पेन्स” इंटर-कटिंग और स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल करने के लिए इसी तकनीक का प्रणेता भी माना जाता है । उनकी इसी फ़िल्म में एक कमाल का चेस सीन भी है जिसमें कार के रीयर व्यू मिरर में पीछा करती हुयी कार दिखायी देती है, यह काफ़ी हद तक सिनेमा के लिए छवियों से और दृश्यों से बनी नयी भाषा लिखने जैसा भी है ।
भारत में जहां सत्तर के दशक तक सोशलिस्ट फ़िल्में मेन्स्ट्रीम सिनेमा में एक अहम हिस्सा थी, अस्सी के दशक में भारतीय सिनेमा की संवेदनशीलता का एक रहस्यमयी पतन हुआ जिस से हम आज भी उबरने की कोशिश कर रहे हैं। फूहड़ता और महिलाओं के वस्तुकरण (ऑब्जेक्टीफ़िकेशन) ने ज़ोर पकड़ा और ब्रेनलेस या मायंड्लेस कहानियों को जनता अपनाने लगी, इसी के प्रतिरोध में भारतीय जन मानस को यथार्थ और आदमियत से जोड़े रखने के लिए पैरलल सिनेमा ने जन्म लिया। गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, सयीद अख़्तर मिर्ज़ा, मनी कॉल और तपन सिन्हा जैसे फ़िल्मकार इस मूव्मेंट के प्रणेता बने।
1993 में आयी सुधीर मिश्रा कृत धारावी फ़िल्म के एक दृश्य में जब ओम् पूरी के किरदार की खून पसीने की मेहनत से बनायी फ़ैक्टरी को उजाड़ दिया जाता है और रघुवीर यादव का किरदार उन्हें सहानुभूति देने उनके पास आता है, ओम् पूरी खीज कर रघु-वीर पर हाँथ उठाता है पर रघुवीर के गालों पर दर्शक कभी थप्पड़ पड़ते देखने के बजाय हम एक कट के बाद अगले दृश्य में ओमपूरी के हाथों से खाने की थाली को अपने से दूर फेंकते हुए देखते हैं।
रेणु सलुजा जैसे कलाकारों का काम एक वृहद् दृष्टि के साथ देखा जाए तो ये कहना ग़लत नहीं होगा की ये सिनेमा की बाउंड्री को पुश करने जैसा है। भानु अथैय्या, सरोज खान और सई परंजपे जैसे कुछ नाम आने वाली ईक्कीसवी सदी की औरतों के लिए एक नयी दिशा का निर्माण कर रहे थे।
दशकों के मेल गेज और हिंसा का जश्न मनाती कहानियाँ और कैमरा का एक तरह इस्तेमाल करने की वजह से एक सिनेमा के चाहने वालों के मन एक ऊब बैठ गयी थी, हीरो की एंट्री हमेशा लो ऐंगल शॉट से होती थी जिसमें आते ही वो मार धाड़ शुरू करता था और हीरोईन की एंट्री कभी किसी को याद ही नहीं रही, या तो उन्हें घर में रहने वाली सीधी साधी लकड़ियों की तरह दिखाया गया या फिर अमीर बाप की ग़ुस्सैल बेटियाँ जिसे गरीब नायक सबक़ सिखाता है, उसका ग़ुरूर तोड़ता है और फिर नायिका उसके प्यार में पड़ जाती है,
1994 की सूपर हिट फ़िल्म “लाड़ला” में अनिल कपूर जो फ़ैक्टरी के मज़दूर का किरदार निभा रहे हैं, फ़ैक्टरी मालिक की बेटी श्री देवी के किरदार को पाँच थप्पड़ मारते हैं जिसमें पहला थप्पड़ उस थप्पड़ का जवाब है जो श्री देवी के किरदार ने उन्हें मारा था, दूसरा थप्पड़ फ़ॉरेन जाकर हिंदुस्तानी सभ्यता को भूल जाने के लिए, तीसरा थप्पड़ उनके घमंड का जुर्माना और चौथा उनकी बदतमीज़ी का सूत और फिर वो पाँचवा थप्पड़ इसलिए मारते हैं क्योंकि उन्हें उनके बदतमीज़ मालिक का दिया हुआ बोनस सूट समेत लौटाना है , इसके बाद अनिल कपूर श्री देवी को अंग्रेज़ी में “यू बैटर अंडरस्टैंड” कहकर स्लो मोशन में कमरे से बाहर जाते हैं
ठीक इसी तरह
1999 में रिलीज़ हुयी अर्जुन पंडित में सनी देओल जूही चावला के घर पहुँच कर उनके पिता को धमकाते हैं की फ़ैशन के नाम पर बेटी को अंग प्रदर्शन करने की आज्ञा देने वाले बाप मत बनो, बेटी जवान होने से पहले ही पूरी दुनिया को दिख जाती है, उसे उछाल उछाल उछाल कर पूरे संसार में बताने की आवश्यकता नहीं” इतना सब सुनने के बाद नायिका के पिता बस यही पूछ पाते हैं की “तुम हो कौन?”
जूही का किरदार जब अर्जुन पंडित का विरोध करते हुए कहती हैं की "मेरा ज़ी जो भी ज़ी चाहेगा मैं वो पहनूँगी, क्या कर लोगे तुम? और उन पर अलमारी से निकाल कर अपने कपड़े फेंकती हैं, अर्जुन पंडित उन्हें अपनी लाल आँखों से घूरने के बाद अपने दोस्त की जेब से लाइटर निकाल कर उनके कपड़े जला देता है और फिर कहानी में आगे उनके शादी के मंडप में ठीक वैसे ही पहुँचते हैं जैसे लाड़ला में अनिल कपूर श्री देवी को थप्पड़ मारने के बाद बाहर निकलते हैं, स्लो मोशन में ।
सिनेमा में ऐसे पात्र लिखने और ऐसे दृश्य दर्शाने के बाद हमेशा सिनेमा रचने वाले यही कहते हैं की वो किरदार ऐसा ही था, या समाज भी तो ऐसा ही होता है, या सिनेमा समाज को आइना दिखलाता है,उनका ये बचाव एकदम खोखला जान पड़ता है क्योंकि वो इस कृत्य की समीक्षा या आलोचना नहीं कर रहे होते हैं वे फ़िल्मकार होने के नाते कैमरे से हीरो की इमेज का जश्न बना रहे होते हैं, और लगातार उसे सही ठहरा रहे होते हैं
ये किसी परिवर्तन के खिलाफ सहमी हुयी पित्रसत्तामकता/पेट्रीआर्की का एक ओछा विरोध था जहां आदमी औरत को हिंसा का सहारा लेकर बार बार याद दिलाता है की उसे उसके संस्कार नहीं भूलने चाहिए, उसे अपना सर ढाँकना ही होगा, उसे बाहर से ज़्यादा अंदर ही रहना होगा
पर यही वो समय है जब कैमरे और लाइट्स की चकाचौंध में ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन जैसी नयी पीढ़ी की हस्तियाँ सिर्फ़ सुंदरता ही नहीं पर अपने आत्म विश्वास से भी वैश्विक मंच पर ये घोषणा कर रही थी की भारत के सोशल फ़ैब्रिक में आने वाले परिवर्तनों को कोई नहीं रोक सकता और औरतें इसमें एक अहम हिस्सा निभाएँगी।
ये उस दशक की कहानियाँ हैं जिस दशक की शुरुआत में देश के प्रधानमंत्री पी॰वी॰ नरसिम्हा राओ और फ़ाइनैन्स मिनिस्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में IMF से सलाह मिलने के बाद भारत में नयी एकनॉमिक -पॉलिसीज़ का आगमन हुआ था और ३४ इंडस्ट्रीस में फ़ोरेन इन्वेस्टमेंट शुरू किया गया, भारत जो अभी तक एक क्लोज़्ड इकॉनमी था अचानक से पूरी दुनिया के लिए खुल गया, विदेश अब बहुत दूर नहीं था
भारत अब एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनने जा रहा था, भारत जिसे पहले से ही उसकी अनेकता के लिए जाना जाता रहा, बीसवीं सदी के आख़री दशक में अब पूरे विश्व के लिए बाहें खोले खड़ा था, उसी तरह फ़िल्मों में कहानी का नायक भी सुंदर वादियों में नायिका के लिए बाहें फैलाए खड़ा था, अब उसमें संवेदनशीलता के कुछ टुकड़े देखे जा सकते थे।
किसी भी प्रकार की कला का एक मक़सद किसी ना किसी तरह खुद को व्यक्त करना होता ही है, और खुद को व्यक्त करते करते आप हमेशा एक पिंजरे को तोड़ते हैं जिसके बहुत सारे पहरेदार हैं। सिनेमा बहुत सारी कलाओं का समागम है पर बार-बार उसे रूढ़िवादिता और कट्टरता से समझौता करते हुए भी पाया गया है, “अर्जुन पंडित” और “लाड़ला” उसी तरह के समझौते हैं।
क्योंकि सिनेमा के माध्यम की डिपेंडेन्सी बाहरी तत्वों पर दूसरी कलाओं से ज़्यादा हैं
मेन्स्ट्रीम सिनेमा हमेशा लोगों को ध्यान में रख कर रचा जाता है, जहां राइटिंग रूम में बार बार लेखक ये सोचते है कि लोग इस दृश्य पर भावुक होंगे, क्रोधित होंगे या उबासी लेंगे, एक तरह से खुद को व्यक्त करने का भाव कहीं पीछे रह जाता है और जन मानस में नयी चेतना जगाने के बजाए सदियों पुरानी अप्रासंगिक सामाजिक मान्यताओं के पुनर्जागरण का ठेका किसी कारण से ही पुरुष पात्रों के कंधों पर रख दिया जाता है शायद इसलिए भी की ये सभी वैल्यू सिस्टम पुरुषों के ही बनाए हुए हैं ।
सत्तर और अस्सी के दशक में कहानी के नायक की ऐंटी-हीरो इमेज बनायी गयी जिसमें उसकी नैतिकता सोशलिस्ट वैल्यूज़ के इर्द गिर्द घूमती थी और वहीं अस्सी के दशक से पतन शुरू हुआ और नब्बे तक पहुँचते पहुँचते ऐंटी-हीरो की छवि लिए नायक मर्यादा और नैतिक मूल्यों की पैरवी करने लगा ।
पर इसी दशक में नयी पीढ़ी के फ़िल्म कार आदित्य चोपड़ा और करण जोहर यूरोप और अमेरिका की नयी दुनिया को खोजते हुए भारत की सभी को अपना सकने की क्षमता में कहानियाँ खोज रहे थे, ग्लोबल वर्ल्ड में नायक और नायिका के प्रेम को नए लेंस से देख़ रहे थे इसके लिए बहुत ज़रूरी था की नायिका को एक अलग पहचान दी जाए, वो ऐसे किरदार का रूप ले जिसके बिना कहानी पूरी नहीं की जा सकती।
अब नायिका पढ़ लिख कर लंदन की ट्रेनों तक तो पहुँच गयी थी पर उसे अब भी जीवन की सम्भावनाओं के बारे में बताने के लिए नायक की ही ज़रूरत थी।
शायद ये वक़्त की ज़रूरत थी की कैमरे के पीछे अपने सभी पात्रों का जीवन निर्धारित करने वाला निर्देशक नहीं एक निर्देशिका हो, पटकथा सिर्फ़ लेखक ही नहीं लेखिका भी लिखें और कैमरामैन एक कैमरा वुमन भी हो सकती है पर अभी एक पुल की ज़रूरत थी, आने वाली पीढ़ी के फ़िल्मकारों का औरतों के किरदारों को लेकर एक नया नज़रिया अपनाना बाक़ी था
इंटर्नेट के आगमन ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया था, हर प्रदेश के बड़े शहरों में यूनवर्सटीज़ और कॉलेजेज़ खुलने लगे थे, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे अपने शहरों को छोड़ बड़ी तादाद में शिक्षा के लिए दूसरे शहर जाने लगे, विचारों का, रहन सहन का, कल्चर का आदान प्रदान भारतीय सोशल फ़ैब्रिक में अप्रतिम था, फ़ेस्बुक और यू-ट्यूब एक क्रांति के जैसे हमारे पास आए और सभी को अपनी बात कहने का मौक़ा मिला, भारत की यंग जनरेशन अपने आप को साबित करना चाहती थी क्योंकि वो अपनी बात रखना जानती थी भले ही वो माध्यम फ़ेस्बुक का स्टैटस हो या एक ट्वीट, इसी दौर की युवा पीढ़ी अपने आप को रिस्क लेने के लिए तैय्यार कर रही थी।
कुछ अतरंगी दिमाग़ थे जो ज़मीन पे नहीं पर इंटर्नेट पे बिज़्नेस करना चाहते थे, अपना स्टार्ट-अप शुरू करना चाहते थे
कुछ बेतुके दिमाग़ जो IITs से पढ़कर विदेश जाने के बजाए देश में पब्लिक सेक्टर में अपनी सेवाएँ देना चाहते थे
कुछ मनचले दिमाग़ जो बिहार, यू.पी के गाँव में बचपन बिताने के बाद सिनेमा के बड़े पर्दे पे अपने क्षेत्र की कहानियाँ कहना चाहते थे,
फ़िल्म की कला जो अभी तक आम जनता के लिए एक तिलिस्म की तरह थी धीरे धीरे वो छवी टूटने लगी, यू ट्यूब पर नो फ़िल्म स्कूल और स्टूडियो बाइंडर जैसे चैनल्ज़ फ़्री में फ़िल्म बनाना सिखा रहे थे.
1991 के बाद फ़ोर्मल सेक्टर में काम कर रही औरतों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ था, जैसा की उस मैग्ज़िन में छपे इंटर्व्यू में उस प्रडूसर ने कहा था कि “जिस दिन औरतें अपने पैसे से टिकट ले पाएँगी, शायद बड़े पर्दे पर औरतों की कहानियाँ भी दिखने लगे”
बेशक अब वो टिकट ख़रीद सकती थी पर नए सिनेमा के जन्म या फिर सिनेमा में नयेपन का इंतेज़ार अब भी था ।ऐसा नहीं है की नयी सदी के आग़ाज़ के बाद तुरंत परिवर्तन दिखने लगे, नए अर्बन इंडिया को नए तरह से कहानी में पिरोने की जद्दोजहद शुरू थी
शाहरुख़ खान अब भी बाहें खोले खड़े थे पर अब एक निर्देशिका के निर्देशन में, सदी के आग़ाज़ के पहले दशक में मेन स्ट्रीम सिनेमा की दो बड़ी फ़िल्में “मैं हुँ ना” और “ओम् शांति ओम्” दोनो फ़राह खान के निर्देशन में बनी थी, जोया अख़्तर “लक बाई चांस” में फ़िल्म इंडस्ट्री के संघर्ष को दिखाने में सक्षम हुयी थी।
एक अप्रत्याशित बदलाव की लहर हिलोरे ले रही थी, पुरुष फ़िल्मकार भी अपने किरदारों को ईक्कीसवी सदी की आधुनिकता और मानवीय गहरायी देने की कोशिश में लगे हुए थे . अनुराग कश्यप नए तरह का सिनेमा खोज रहे थे, लोगों के सामने पेचीदा किरदार परोस रहे थे, वहीं इम्तियाज़ अली की कहानियों में औरतों के पात्र एक अनदेखी ताज़गी से लिप्त थे जिसमें उनका आत्म विश्वास उनके पात्र की सबसे बड़ी ताक़त थी
2007 में इम्तियाज़ अली निर्देशित “जब वी मेट” में जब करीना के किरदार को पता चलता है की शाहिद के किरदार की प्रेमिका उन्हें छोढ़ कर ज़ा चुकी है तो वो उन्हें उनके बटुए में रखी प्रेमिका की तस्वीर को जलाकर कर बाथरूम में फ़्लश करने की हिदायत देती हैं और ऐसा करने के शाहिद कहते हैं की “ये बहुत बेवक़ूफ़ी का काम था पर मुझे वाक़ई अच्छा लग रहा है”, संवाद में आगे करीना उन्हें समझाती हैं की दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें कोई भी पसंद कर लेगा, क्योंकि वो हैंडसम हैं, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं होता तो मै भी कर लेती”
जब शाहिद उनसे पूछते हैं की “ तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? ” तो करीना जवाब देती हैं की “बहुत, मै अपनी फ़ेवरेट हुँ”
बॉलीवुड मेन-स्ट्रीम सिनेमा में नायिका का एक दृढ़ आवाज़ में यह कहना की “मैं अपनी फ़ेवरेट हुँ” मील के पत्थर जैसा साबित हुआ, युवा पीढ़ी को अपने आप पे और अपनी क्षमताओं पर भरोसा था और कुछ भी कर लेने की हिम्मत।
2009 में देव डी के एक दृश्य में माही गिल का किरदार अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी आतुर हो जाती है की सायकल पर गद्दे बाँध कर खेत पहुँच जाती है और अपने प्रेमी का इंतेज़ार करती है।
सिनेमा की नायिका अब नायक की हौसला अफजाई कर रही थी और उसे जीवन की अनंत सम्भावनाओं से अवगत करवा रही थी।
अनुराग की ही पिरीयड फ़िल्म “गैंज़ ओफ़ वसीपुर” के दूसरे भाग में नवाज़ का किरदार नायिका के साथ एक तालाब के पास बैठा हुआ होता है और धीरे से नायिका के हाथों पर हाँथ रख देता है, नायिका उसे तुरंत याद दिलाती है की “ऐसे अच्छा थोड़ी ही लगता है आपको पर्मिशन लेनी चाहिए ना” नवाज़ जो फ़िल्म में गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, नायिका से डाँट खाकर रोने लगते हैं।
नीरज घेयवान मेंस्ट्रीम में ऐसी कहानियाँ लेकर आए जो समाज में फैले जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और सोशल फैबरिंक को कालपनिकता में बखूबी पिरोती हैं, मसान में भी ब्राह्मण परिवार से आने वाली देवी पाठक अपने दुखों से लड़ने की कोशिश कर रही है, मर्दों की नज़र और अपने पिता की नफ़रत से लड़ रही है, और उसे कैसे भी करके अपने शहर से बाहर निकलना है वहीं दूसरी ओर दलित समुदाय से आने वाले दीपक अपनी प्रेमिका को अपनी पहचान बताने में कतराता है, फ़िल्म के एक दृश्य में जब जब शालू दीपक से पूछती है की अब तुम कहाँ जाओगे, दीपक उसे अपना सही पता बताने में कतराता है फिर एक खीज के साथ उसे बताता है की वो हरीश चंद्रा घाट पे रहता है, उसके बाप दादा पीढ़ियों से लाशें जलाते आए हैं और वो भी यही करता है। अक्सर हमारी दबी हुयी कुंठाएँ और शर्म ऐसे ही बाहर आती हैं, साधारण बोल चाल में नहीं।
घेयवान की फ़िल्म गीली पुच्ची में जब कोंकना का किरदार जो दलित वर्ग से हैं, जब अदिति राओ हैदरी के घर जाता है तो उन्हें अलग गिलास में चाय परोसी जाती है, कोंकना की आँखों के साथ साथ निर्देशक भी कैमरे से इस उच्च जाती के घरों में घटने वाली इस त्रासदी को एक नए और ज़रूरी लेन्स से देखते हैं, घेयवान का सिनेमा पूरे समाज को अपने भीतर पूरी ख़ूबसूरती और ख़ामियों के साथ समेटे हुए है । कथानक की कल्पना में लैंगिक भेदभाव, जातीय समीकरण और सामाजिक यथार्थ गुथा हुआ है, घेयवान का सिनेमा अपने समकालीन फ़िल्मकारों से ज़्यादा संवेदनशील और संजीदा जान पड़ता है जिसमें हर बार याद दिलाया जाता है की सामाजिक तत्व होने से पहले हम एक मनुष्य हैं और शायद प्रेम हमें बचा सकता है।
इसी तरह के संजीदा और संवेदनशील सिनेमा में आज भारत की बहुत सी महिला फ़िल्मकार मुख्यधारा में लगातार अपनी कहानियाँ कह रही हैं
कोंकोना सेन शर्मा की “ अ डेथ इन द गंज” एक मार्मिक फ़िल्म है जो भावुकता से कही गयी भावो के अभाव की कहानी है, इस फ़िल्म की अंतिम छवी को अपनी चेतना से दूर कर पाना लगभग असम्भव है। उस दृश्य के बारे में यहाँ बात करना ठीक नहीं, क्योंकि अच्छा सिनेमा देखने से ज़्यादा अनुभव करने के लिये बनाया जाता है ।
असम की फ़िल्मकार रीमा दास एक के बाद एक ऐसी फ़िल्में रच रही हैं जो माँ की सुनायी हुयी या जी हुयी कहानियों या उनके संघर्षो के बहुत पास है। रीमा अपनी फ़िल्में लिखती हैं, डिरेक्ट करती हैं और शूट और एडिट भी खुद करती हैं। उनकी बहू चर्चित फ़िल्म “विलेज रॉक स्टार्स” में उनकी क्रू में शायद बस दो लोग थे। पूरा गाँव उनका सेट था और गाँव के बच्चे ऐक्टर। 2017 में इस फ़िल्म को नैशनल अवार्ड से नवाज़ा गया था । रीमा इसी तर्ज़ पे दो और फ़िल्मों का निर्माण कर चुकी हैं।
रीमा और कोंकोना के साथ गौरी शिंदे, अश्विनी इय्यर तिवारी, अलंकृता श्रीवास्तव, रीमा कागती, जोया अख़्तर लगातार सफल फ़िल्मों का निर्माण करते आ रही हैं । निर्देशन के क्षेत्र में ही नहीं पर सिनेमा से जुड़ी हर फ़ील्ड में औरतों ने अपना रोल बदला है
गुनीत मोंगा एक प्रोड्यूसर के तौर पर दो अकैडमी अवार्ड जीत चुकी हैं, सिनेमटोग्राफ़ी के क्षेत्र में श्रेया देव दुबे, अर्चना घांग्रेकर, एडिटिंग में संयुक्ता काजा, आरती बजाज, श्वेता मैथ्यू आज बड़े नाम हैं।
पिछले कुछ वर्षों में आए सिनेमा में बहुत सी वैसी कहानियाँ मिली यह उन कहानियों का कहने का ढंग मिला जैसे माँ सुनाया करती थी। ऐसा नहीं है की जिस तरह की फ़िल्में बॉलीवुड में बनती हैं उनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, अभी भी उसी तर्ज़ पर मर्दानगी को परोसा जा रहा है जैसे आज से दो दशक पहले परोसा ज़ा रहा था, कबीर सिंह आज भी प्रेम में पागल होकर प्रीति को थप्पड़ मार सकता है और दर्शक खुश होते हैं पर कुछ ऐसे कहानीकारों को आगमन हुआ है जो धीरे धीरे अपनी गति से परिवर्तन ला रहे हैं, जो संवेदना का सिनेमा रच रहे हैं, जो फ़िल्में बनकर असंख्य लोगों की मदद कर रहे हैं, जो बहुत प्रेम से आपको अपनी कल्पना की दुनिया में लेकर चले जाते हैं और आप उन के हाथों में बहुत महफ़ूज़ महसूस करते हैं , यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं की औरतों की कहानियाँ औरतें ही कहें, पुरुषों की कहानियाँ पुरुष ही कहें, ज़रूरी हैं कहानियों की ज़िम्मेदारी को समझना और हर किरदार को एक ज़रूरी गम्भीरता के साथ रचना क्योंकि कहानियाँ कहना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हज़ारों लाखों लोग सिनेमाघरों के कोने में बैठ कर चुप चाप अपने आप को किरदारों में ढूँढते हैं और उनसे अपनी असमर्थताओं को समझते हैं या अपनी शिकायतों का जवाब माँगते हैं। हम बड़े पर्दे पर नायिका और नायक में कुछ ऐसा ढूँढते हैं जो हमारी क्षमताओं के परे हैं और सिनेमा घर से बाहर निकलते ही हम उसी असंभवता के पास धीरे धीरे पहुँचने की कोशिश करते हैं।